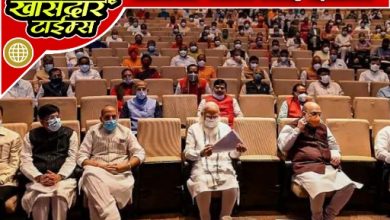– विशेष संपादकीय
नफ़रत को पहचानना और उसे नाम देना किसी समाज के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में बीते एक दशक में यह चुनौती पुलिस, न्यायपालिका और चुनाव आयोग के लिए जटिल होती गई है। खासकर जब नफरत को राजनीतिक और कानूनी संरक्षण मिलने लगे, तो उसे पहचानने और उस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह का हालिया फैसला इस संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने 2020 के चुनावी भाषणों में नफरत फैलाने के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायपालिका और नफरत फैलाने वालों की जवाबदेही
न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मिश्रा ने अपने भाषणों में ‘मिनी पाकिस्तान’ और ‘भारत-पाकिस्तान की लड़ाई’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की सोची-समझी रणनीति थी।
लेकिन यह पहली बार नहीं है जब भारत की न्यायपालिका ने ऐसे मामलों में ढुलमुल रवैया अपनाया है। जब भी भाजपा और उससे जुड़े नेताओं के घृणा फैलाने वाले बयानों की जांच की जाती है, तब अक्सर न्यायपालिका और पुलिस का एक बड़ा हिस्सा या तो इन मामलों को नजरअंदाज कर देता है या फिर उन पर ढील बरतता है।
2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए, तब भाजपा नेता कपिल मिश्रा के उकसाने वाले भाषणों पर तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद उनका तबादला कर दिया गया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि सत्ता में बैठे लोग नफरत फैलाने वाले अपने नेताओं को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर सकते हैं।
भाजपा नेताओं की बयानबाजी और चुनाव आयोग की चुप्पी
भारत में नफरत की राजनीति अब कोई अपवाद नहीं रही, बल्कि यह भाजपा और उससे जुड़े संगठनों की चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुलेआम विभाजनकारी बयान दिए। उन्होंने ‘ग़रीबों के पैसे को कांग्रेस के इशारे पर मुसलमानों को देने’ जैसी बातें कहीं, लेकिन न तो चुनाव आयोग और न ही पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की।
चुनाव आयोग की भूमिका भी चिंताजनक है। यह वही आयोग है जिसने विपक्षी दलों के नेताओं पर मामूली बयानबाजी के लिए कार्रवाई की, लेकिन जब भाजपा के नेता खुलेआम घृणास्पद भाषण दे रहे थे, तब उसने आँखें मूँद लीं। यह स्पष्ट करता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह कमजोर किया जा रहा है और उन्हें एक राजनीतिक दल के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है।
अदालतों की भूमिका: दोहरा रवैया क्यों?
दिल्ली की अदालत ने कपिल मिश्रा के मामले में नफरत को नफरत कहने की हिम्मत दिखाई, लेकिन यह एक दुर्लभ उदाहरण है। आमतौर पर, अदालतें और कानून व्यवस्था से जुड़े संस्थान ऐसे मामलों में कार्रवाई करने से बचते हैं।
हाल ही में, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक मस्जिद में घुसकर दो लोगों ने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए। इस पर पुलिस ने घृणा फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया कि ‘जय श्रीराम’ एक धार्मिक नारा है और इससे किसी की भावनाएँ आहत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने यह सवाल पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि वे लोग मस्जिद में क्यों घुसे और वहाँ जाकर नारे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
क्या वे मुसलमानों को रामभक्ति का संदेश देने गए थे? या फिर यह एक सोची-समझी रणनीति थी जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बनाया जा सके? यह सवाल अदालत ने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की।
मीडिया की चुप्पी: कौन जिम्मेदार है?
नफरत फैलाने वालों की जवाबदेही केवल अदालतों और पुलिस की ही नहीं बनती, बल्कि मीडिया का भी दायित्व होता है कि वह ऐसे मामलों को उजागर करे और सत्ता को जवाबदेह बनाए। लेकिन भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा आज सत्ता का भोंपू बन चुका है।
कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा जैसे नेताओं ने जब ‘देश के ग़द्दारों को, गोली मारो’ जैसे नारे लगवाए, तब यह सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि यह नफरत के एक बड़े अभियान का हिस्सा था। लेकिन भारतीय मीडिया ने इसे नजरअंदाज किया। संपादकीयों में इस पर कोई आलोचना नहीं की गई, न ही टीवी डिबेट में इसे एक गंभीर मुद्दा माना गया।
नफरत की जड़ें: बच्चों तक कैसे पहुँची?
अगर हम इस नफरत को रोकने में नाकाम रहते हैं, तो इसका सबसे बुरा असर अगली पीढ़ी पर पड़ेगा।
पुणे की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि जब वे बच्चों के साथ ऑटो में सफर कर रही थीं, तो जैसे ही ऑटो एक मस्जिद के सामने पहुँचा, बच्चों ने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने यह नारा किसी धार्मिक आस्था से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि एक सांप्रदायिक उद्देश्य से लगाया।
इसी तरह, मध्य प्रदेश में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि जब वे और उनकी हिजाब पहनने वाली मित्र एक कार्यशाला से लौट रही थीं, तो कुछ हिंदू बच्चों ने उनकी मुस्लिम मित्र को देखकर ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाया। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह घृणा धीरे-धीरे समाज के बच्चों तक पहुँच रही है और एक पूरे समुदाय के प्रति अविश्वास और नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है।
पटना के एक स्कूल की एक अध्यापिका ने बताया कि जब वे कक्षा में पहुँचीं तो ब्लैकबोर्ड पर पहले से ही लिखा था – ‘मंदिर वहीं बनाएँगे।’
इन घटनाओं को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या अब भारतीय समाज की नयी पीढ़ी भी सांप्रदायिक घृणा से ग्रसित हो रही है?
निष्कर्ष: क्या नफरत को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएँगे?
यह स्पष्ट है कि भारत में नफरत केवल व्यक्तिगत विचारधाराओं का हिस्सा नहीं रह गई है, बल्कि यह अब एक संगठित राजनीतिक और सामाजिक परियोजना बन चुकी है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया, तो इसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।
आज हमें न्यायाधीश जितेंद्र सिंह जैसे ईमानदार और निष्पक्ष लोगों की ज़रूरत है, जो नफरत को नफरत कहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ न्यायपालिका की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। जब तक आम नागरिक, मीडिया और संवैधानिक संस्थाएँ मिलकर इस नफरत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक यह कैंसर और गहराई तक फैलता जाएगा।
अब सवाल यह है कि क्या हम इस नफरत को पहचानने और उसे खत्म करने के लिए आगे आएंगे? या फिर इसे अपनी नई पीढ़ी का स्वाभाविक व्यवहार बनने देंगे?
– विशेष संपादकीय, खासदार टाइम्स